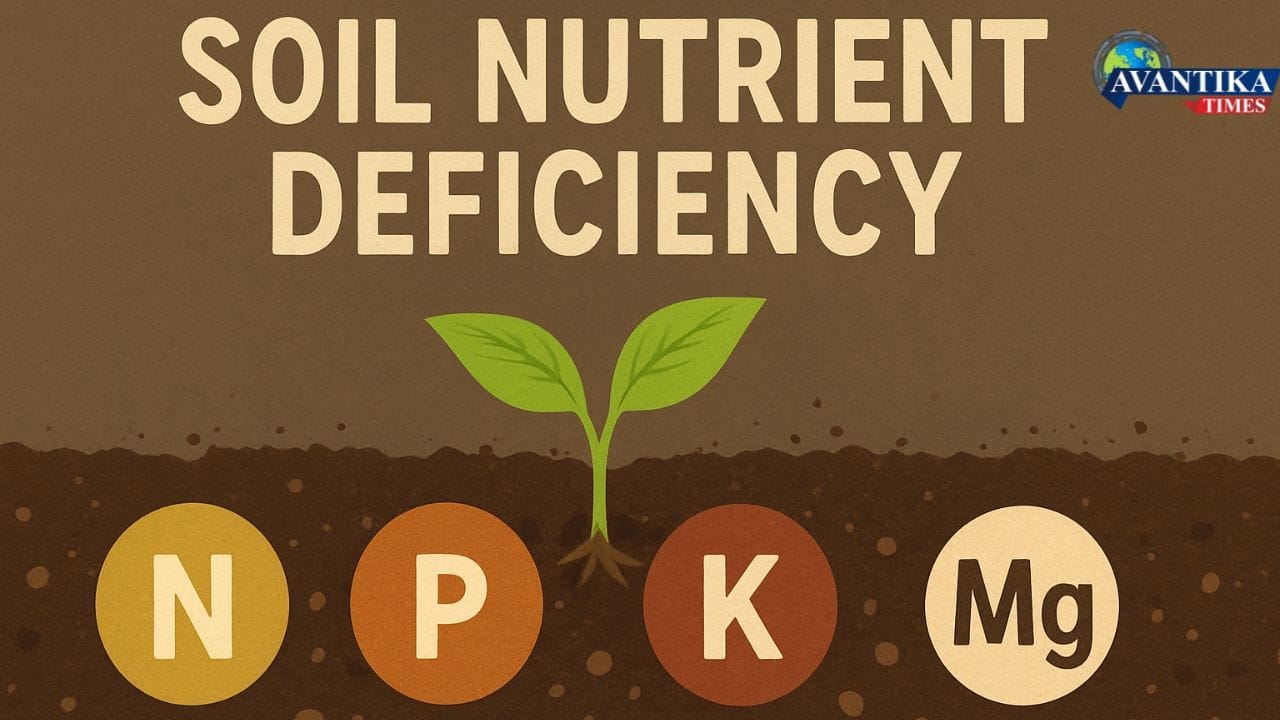पराली न जलाएं – जानिए इसके विकल्प और सरकार की सहायता

Contents
-: Smart Farming Techniques :-
हर साल जब धान की फसल कटाई के बाद खेतों में पराली (फसल अवशेष) बचती है, तो कई किसान उसे जलाने का आसान लेकिन हानिकारक उपाय चुनते हैं। इससे न केवल वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि होती है, बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है। दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में धुंध और प्रदूषण का प्रमुख कारण पराली जलाना ही माना जाता है।
पराली जलाने से नुकसान:
हवा में PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ जाती है।
श्वसन संबंधी रोगों में वृद्धि होती है – अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी।
मिट्टी के लाभकारी जीव नष्ट हो जाते हैं जिससे उपज में गिरावट आती है।
आसपास की जैव विविधता को खतरा होता है।
पराली का समाधान – वैकल्पिक उपयोग:
बायो-डीकंपोज़र स्प्रे:
दिल्ली सरकार ने IIT दिल्ली और PUSA संस्थान के साथ मिलकर एक बायो-डीकंपोज़र स्प्रे विकसित किया है, जो पराली को खेत में ही खाद में बदल देता है।हैप्पी सीडर मशीन:
यह मशीन बिना पराली हटाए ही गेहूं की बुआई कर सकती है। इससे किसान को पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।बैलर और रेक मशीनें:
ये मशीनें पराली को इकट्ठा करके गट्ठर बना देती हैं, जिसे ईंधन या पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।बायो गैस और पेपर इंडस्ट्री:
कई स्थानों पर पराली को बायोगैस प्लांट में ईंधन या कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
सरकार की सहायता योजनाएँ:
सबसिडी योजना: कृषि यंत्रों जैसे हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम आदि पर 50% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
कस्टम हायरिंग सेंटर: छोटे किसानों को मशीनें किराए पर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें इन केंद्रों की स्थापना कर रही हैं।
प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान: कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए नियमित प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।
निष्कर्ष:
पराली जलाना एक अस्थायी समाधान है जो दीर्घकालिक संकट को जन्म देता है। अगर हम स्वच्छ हवा, स्वस्थ मिट्टी और बेहतर पर्यावरण की कामना करते हैं तो हमें आधुनिक और टिकाऊ विकल्प अपनाने होंगे। किसान भाईयों से निवेदन है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का सदुपयोग करें और पराली जलाने से परहेज करें।
प्रेरणादायक कहानियाँ: सफल किसान, सफल समाधान
पंजाब के मानसा जिले के किसान गुरप्रीत सिंह की कहानी
गुरप्रीत सिंह ने पराली जलाने की बजाय ‘सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम’ का प्रयोग किया। उन्होंने गेहूं की बुआई बिना पराली हटाए की और पाया कि फसल की उपज में कमी नहीं आई, बल्कि मिट्टी की नमी बनी रही। आज उनके गांव के 20 से अधिक किसान इस पद्धति को अपना चुके हैं।
हरियाणा के करनाल की महिला किसान सुनीता देवी
सुनीता देवी ने बायो-डीकंपोज़र का उपयोग करते हुए खेत में ही पराली को जैविक खाद में बदला। उन्होंने यह खाद आसपास के किसानों को भी बेची और एक नया आय का स्रोत बना लिया।
स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायतों की पहल
यह भी पढ़े :-
मल्चिंग से बदलेगी किसानी की तस्वीर – नमी भी बचे, खरपतवार भी हटे!
गांव स्तर पर निगरानी समितियाँ: कई जिलों में ग्राम पंचायतों ने पराली जलाने पर निगरानी के लिए समितियाँ बनाई हैं जो किसानों को जागरूक करती हैं और वैकल्पिक उपायों की जानकारी देती हैं।
स्कूल और कॉलेजों की सहभागिता: युवाओं द्वारा बनाए गए एनवायरनमेंट क्लब गांवों में जागरूकता रैलियाँ और नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं।
‘नो पराली जलाओ’ संकल्प अभियान: कई राज्यों में किसानों से पराली न जलाने की शपथ ली जा रही है, और उन्हें प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित भी किया जाता है।
क्या करें और क्या न करें
| क्या करें ✅ | क्या न करें ❌ |
|---|---|
| बायो-डीकंपोज़र या कृषि यंत्रों का उपयोग करें | खेतों में पराली न जलाएं |
| ग्राम पंचायत और कृषि विभाग से जुड़ें | सब्सिडी योजनाओं की अनदेखी न करें |
| दूसरे किसानों को भी प्रेरित करें | शॉर्टकट को अपनाकर पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएं |
जनता की भागीदारी – आप क्या कर सकते हैं?
पराली जलाना केवल किसानों की समस्या नहीं है – यह एक सामूहिक पर्यावरणीय संकट है जिसमें समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी बनती है। आम नागरिक, विद्यार्थी, सामाजिक संगठन, और मीडिया यदि मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है।
आपका योगदान हो सकता है:
किसानों को पराली जलाने के नुकसान और विकल्पों के बारे में जागरूक करना।
सोशल मीडिया पर सूचना और सकारात्मक उदाहरण साझा करना।
गांवों में जागरूकता कार्यक्रम और अभियान में भाग लेना।
स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर संवाद स्थापित करना।
कानूनी प्रावधान और दंड
पराली जलाना वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। राज्य सरकारें और NGT (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने इस पर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
प्रमुख प्रावधान:
पराली जलाने पर ₹2,500 से ₹15,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है, जो क्षेत्र और दोहराव पर निर्भर करता है।
गंभीर मामलों में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
सब्सिडी और सरकारी सहायता से वंचित किया जा सकता है।
निष्कर्ष और अपील
पराली प्रबंधन केवल एक तकनीकी विषय नहीं, बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का विषय है। यदि हर किसान, नागरिक और अधिकारी मिलकर काम करें, तो भारत स्वच्छ हवा और उन्नत कृषि की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है।
किसानों से निवेदन है कि पराली जलाने की बजाय उपलब्ध वैकल्पिक उपायों को अपनाएं।
नागरिकों से अनुरोध है कि वे जागरूकता फैलाएं और स्थानीय स्तर पर इस आंदोलन का हिस्सा बनें।
“स्वस्थ किसान, स्वच्छ खेत, और साफ़ हवा – यही है नए भारत की पहचान!”
सारांश: एक नज़र में पराली प्रबंधन
पराली जलाना वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य संकट और मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है।
सरकार ने मशीनों, स्प्रे, और जागरूकता के माध्यम से कई समाधान उपलब्ध कराए हैं।
किसानों को अब पराली जलाने की बजाय उसे संसाधन के रूप में देखने की जरूरत है।
जनता, पंचायतें, और युवा मिलकर इस परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
प्रेरणात्मक उद्धरण और संदेश
“धरती हमारी मां है, पराली जलाना उसे जलाने जैसा है।”
“खेती में नवाचार ही पर्यावरण का सम्मान है।”
“यदि हम आज हवा को नहीं बचाएंगे, तो कल हवा हमें नहीं बचाएगी।”
अंतिम अपील: आइए एक साथ कदम बढ़ाएं
पराली प्रबंधन की इस यात्रा में हर व्यक्ति का सहयोग ज़रूरी है। चाहे आप किसान हों, शिक्षक, छात्र या प्रशासनिक अधिकारी – आपका एक छोटा-सा कदम भी पर्यावरण को बचाने में बड़ा बदलाव ला सकता है।
“आइए, संकल्प लें – पराली नहीं जलाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे!”
जुड़िये हमारे व्हॉटशॉप अकाउंट से- https://chat.whatsapp.com/JbKoNr3Els3LmVtojDqzLN
जुड़िये हमारे फेसबुक पेज से – https://www.facebook.com/profile.php?id=61564246469108
जुड़िये हमारे ट्विटर अकाउंट से – https://x.com/Avantikatimes
जुड़िये हमारे यूट्यूब अकाउंट से – https://www.youtube.com/@bulletinnews4810